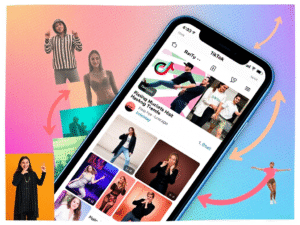सितार की मधुर तान सुनकर क्या आपने कभी सोचा है कि इस वाद्य को बजाने वाले पहले कलाकार कौन थे? या फिर यह खूबसूरत वाद्य यंत्र भारत आया कैसे? सितार न सिर्फ़ भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रतीक है, बल्कि यह फ़ारसी संस्कृति और भारतीय कला का अनूठा संगम भी है। इस लेख में, हम सितार के रहस्यमय इतिहास को उजागर करेंगे—अमीर खुसरो के दावों से लेकर आधुनिक युग के महान सितार वादकों तक की पूरी यात्रा पर चलेंगे।
1. सितार का उद्गम: फ़ारसी ‘सेतार’ या भारतीय ‘वीणा’?
सितार की उत्पत्ति पर विद्वानों में बहस सदियों से चल रही है।
1.1. फ़ारसी संगीत का प्रभाव
- सेतार से सितार तक: फ़ारसी शब्द “सेतार” (तीन तार) से सितार नाम की उत्पत्ति।
- मुग़ल काल में परिवर्तन: फ़ारसी वाद्यों जैसे ‘तंबूर’ और ‘सेतार’ को भारतीय वीणा के साथ मिलाकर नया स्वरूप दिया गया।
1.2. भारतीय वीणा का योगदान
- रुद्र वीणा की छाया: सितार की लंबी गर्दन और तुम्बे की डिज़ाइन प्राचीन वीणा से प्रेरित है।
- 19वीं सदी का नवीनीकरण: मसीत खाँ द्वारा सितार में “गुलाब” (अतिरिक्त तार) जोड़े गए।
2. अमीर खुसरो: सितार के जनक या मिथक?
13वीं सदी के संगीत प्रेमी अमीर खुसरो को अक्सर सितार का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन क्या यह सच है?
2.1. ऐतिहासिक दावे
- पहला उल्लेख: खुसरो ने “तुतियानामा” में “त्रितंत्री वीणा” (तीन तार वाले वाद्य) का ज़िक्र किया, जो सितार का प्रारंभिक रूप हो सकता है।
- किंवदंती: कहा जाता है कि खुसरो ने वीणा को संशोधित करके सेतार जैसा वाद्य बनाया।
2.2. विवाद और सच्चाई
- साक्ष्य की कमी: खुसरो के समय सितार जैसे वाद्य के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते।
- विद्वानों की राय: डॉ. लालमणि मिश्र जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि सितार 18वीं सदी में विकसित हुआ, न कि खुसरो के समय।
3. सितार का विकास: मध्यकाल से आधुनिकता तक
सितार ने भारत में आकर कैसे अपनाया नया स्वरूप?
3.1. मुग़ल दरबारों में संरक्षण
- तानसेन के युग में: अकबर के दरबार में सितार जैसे वाद्यों को प्रोत्साहन मिला।
- लखनऊ और रामपुर घराने: 19वीं सदी में इन घरानों ने सितार वादन की नई शैलियाँ विकसित कीं।
3.2. 20वीं सदी: सितार का स्वर्ण युग
- पंडित रविशंकर: विश्व पटल पर सितार को पहचान दिलाने वाले महान कलाकार।
- विलायत खाँ: गायकी अंग (गायन जैसी शैली) को सितार में लाने का श्रेय।
4. सितार की संरचना: विज्ञान और कला का मेल
सितार बनाने की प्रक्रिया में छिपे हैं अनूठे रहस्य।
4.1. प्रमुख भाग और उनका महत्व
- तुम्बा: लौंग के आकार का निचला हिस्सा, जो ध्वनि को गूँज देता है।
- दंड (गर्दन): 20-22 पर्दे (मेटल फ़्रेट्स) लगी लकड़ी की लंबी गर्दन।
- तार: मुख्य तार (बाज और चिकारी) और सहायक तार (सिम्बल)।
4.2. निर्माण की सामग्री
- लकड़ी: ट्यूनिंग के लिए सागौन या टीक की लकड़ी।
- चमड़ा: तुम्बे पर लगा बकरी का चमड़ा।
5. सितार वादन की शैलियाँ: घरानों की विरासत
सितार पर अलग-अलग घरानों की अपनी विशिष्ट शैली है।
5.1. मैहर घराना
- पंडित रविशंकर: ध्रुपद अंग और तंत्रकारी का समन्वय।
5.2. इंदौर घराना
- उस्ताद विलायत खाँ: गायकी अंग में भावनात्मक अभिव्यक्ति।
6. सितार का वैश्विक प्रभाव: पश्चिम तक पहुँच
- द बीटल्स और जॉर्ज हैरिसन: 1960 में रविशंकर से प्रभावित होकर सितार को पश्चिमी संगीत में शामिल किया।
- फ्यूज़न संगीत: अनुष्का शंकर और नोराह जोन्स का प्रयोग।
निष्कर्ष
सितार का इतिहास एक पहेली की तरह है—जहाँ फ़ारसी सेतार, भारतीय वीणा, और मध्यकालीन प्रयोगों के धागे आपस में गुथे हैं। हालाँकि अमीर खुसरो को “जनक” मानने में विवाद है, पर इसमें कोई शक नहीं कि सितार भारतीय संगीत की आत्मा बन चुका है। यह लेख नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेज़ है!